-बढ़ती एलर्जी के लिए बाहरी प्रदूषण के साथ ही अंदरूनी प्रदूषण भी जिम्मेदार
-आयोजित संगोष्ठी में पहुंचे स्पेन से आये विश्व एलर्जी संगठन के अध्यक्ष

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। भारतीय उप-महाद्वीप में विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास अलग-अलग एलर्जी है। एलर्जी को भड़काने में आर्द्रता यानी नमी प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे आर्द्रता बढ़ती जाती है, नए नए फफूंद और धूल के कण अधिक हानिकारक होते जाते हैं। बढ़ता प्रदूषण भी पराग के एलर्जेनिक गुणों को बढ़ा देता है।
यह बात स्पेन से आये हुय विश्व एलर्जी संगठन के अध्यक्ष डा0 इग्नेशियो जे. अंसोतेगुई ने यहां एक होटल में शुक्रवार को आयोजित संगोष्ठी में कही। लखनऊ चेस्ट क्लब एवं उ0प्र0 चेप्टर, इण्डियन चेस्ट सोसाइटी द्वारा वायु प्रदूषण एवं एलर्जी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ में डा0 सूर्यकान्त, विभागाध्यक्ष, रेस्परेटरी मेडिसिन विभाग, के.जी.एम.यू. की अध्यक्षता में किया गया था। इस संगोष्ठी में जाने माने फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, चेस्ट रोग विशेषज्ञ एवं पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित रहे।
इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि स्पेन से आये हुय विश्व एलर्जी संगठन के अध्यक्ष डा0 इग्नेशियो जे. अंसोतेगुई ने एलर्जी के वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर बोलते हुए वायु प्रदूषण की वजह से मानव स्वास्थ पर होने वाले दुष्प्रभाव एवं एलर्जी के रोगों और कारकों पर अपने विचार एवं शोध प्रस्तुत किये। उन्होंने एलर्जी रोगों को प्रभावित करने वाले एलर्जी के विभिन्न कारणों, प्रेरक पदार्थो तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों की विस्तृत चर्चा की।
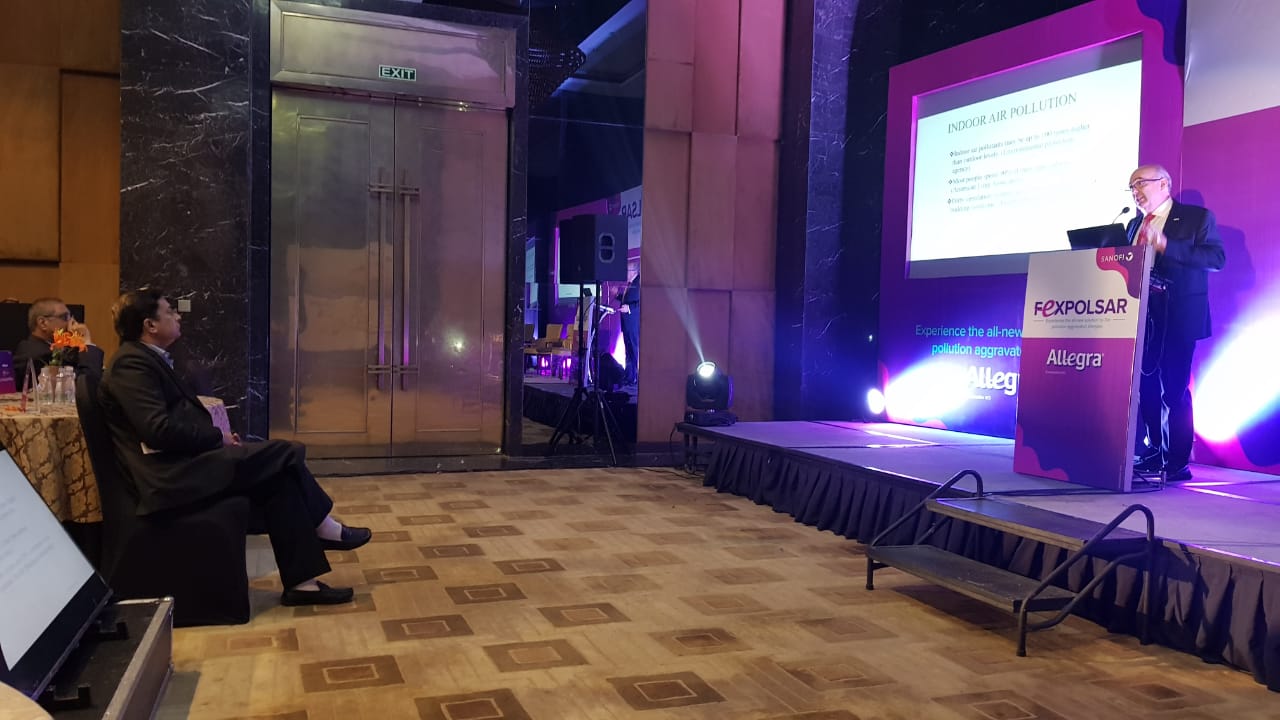
डा0 इग्नेशियो ने बताया कि प्रदूषण दुनिया भर में मृत्यु और बीमारी का सबसे बड़ा पर्यावरणीय कारण है, दहनशील ईंधन के जलने और बायोमास ईंधन के कारण लगभग 85 प्रतिशत वायु प्रदूषण फैलता है। चिकित्सा विज्ञान के अध्ययनों ने वायु प्रदूषकों और एलर्जी या श्वसन लक्षणों में वृद्धि के बीच संबंध दिखाया है। उन्होंने बताया कि बढ़ते प्रदूषण से हवा में पराग कणों की संख्या बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप एलर्जी पैदा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि बाहरी वायु प्रदूषण के अलावा, आंतरिक वायु प्रदूषण में वृद्धि भी बढ़ती हुयी एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। घरेलू सफाई में इस्तेमाल होने वाले रसायनिक पदार्थ, स्प्रे और मच्छर निरोधी कॉइल्सके अंधा-धुंध उपयोग से भी एलर्जी पैदा होती है। जलवायु परिवर्तन से भी एलर्जी रोगों की वृद्धि होती है। दुनिया में प्रतिवर्षलगभग 42 लाख लोग प्रदूषित वायु के कारण और 38 लाख लोग चूल्हे पर खाना बनाने के कारण मृत्यु का शिकार हो रहे हैं।उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यूरोप की आधी जनसंख्या वायु प्रदूषण से होने वाले एलर्जिक बीमारियों से पीड़ित होगी।
इस विषय में भारतीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुये इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एवं एप्लाइड इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 सूर्यकान्त ने बताया कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर भारत (कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा और गुड़गांव) से हैं। जिनमें कानपुर (पीएम 2.5 – 173 मिलीग्राम प्रति मिमी)सबसे प्रदूषित शहर है।

डा0 सूर्यकान्त ने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करती है। घटता हुआ वन आवरण वायु प्रदूषण के इस प्रभाव को और भी बढ़ाता है। पिछले 50 वर्षों में भारत में 50 प्रतिशत वन आवरण नष्ट हो गया है। ग्रामीण वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान चूल्हे पर भोजन पकाने द्वारा उत्पन्न उत्सर्जनों का होता है। इनकी सान्द्रता कोयला जलने से उत्पन्न सान्द्रता से 5 गुना अधिक होती है। ग्रामीण स्त्रियों में चूल्हे पर खाना बनाने से श्वास सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर रोग से ग्रसित होने का खतरा ज्यादा होता है। विश्व में लगभग 3 अरब लोग अभी भी खाना पकाने के लिए खुले में ठोस ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग करते हैं। तंबाकू का धुआं भी एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता बन रहा है।
भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 12 लाख व्यक्तियों की मौतें होती हैं। दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 35000 व्यक्तियों की मृत्यु वायु प्रदूषण से जनित रोगों की वजह से हो जाती है। दिल्ली की हवा में 24 घण्टे सांस लेने से व्यक्ति एक दिन में 50 सिगरेट के समान धुओं का सेवन करता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया,अधिक रक्तचाप का खतरा, कैंसर, मानसिक मंदता, चिंता, बालों का झड़ना, बांझपन, गर्भपात, ओजोन परत की कमी तथा भूमि की उर्वरता भी कम हो जाती है।शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर तीन भारतीयों में से एक एलर्जी से पीड़ित है,वे बस इसे आम सर्दी या खांसी का रूप समझते हैं।

उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण वायुमंडल की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करता है। वायुमंडल में प्रमुख वायु प्रदूषक कण पदार्थ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाईऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कणों के रूप में मौजूद हैं। वाह्य प्रदूषण के दो मुख्य स्रोत परिवहन और उद्योग जनित प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषण फैलाने में आधे से अधिक योगदान परिवहन तन्त्र का है जबकि 10 प्रतिशत से अधिक योगदान उद्योग उत्सर्जन का है।
डा0 सूर्यकान्त ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के 20 शहरों में पर्यावरण जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एकराष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य प्रोफाइल अध्ययन की शुरूआत 2019 में की है। इस अध्ययन का उद्देश्य वायु प्रदूषण की वजह से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करना है। इसमें से कानपुर शहर में होने वाला अध्ययन उनके नेतृत्व में चल रहा है।
डा0 सूर्यकान्त ने वायु प्रदूषण की समस्या को नियन्त्रित करने के लिए बताया कि समाज को व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि, फूलों के गुलदस्ते के बजाय पौधों को भेंट स्वरूप देना, पैदल चलने और साइकिल का उपयोग करना तथा धूम्रपान के उन्मूलन का सुझाव दिया।प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे विभिन्न समूहों के साथ, देश के डाक्टरों ने सामाजिक संगठन ”डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर” (डीएफसीए) की शुरूआत की है।इसका उद्देश्य डॉक्टरों को प्रेरित करने के लिए ’चैंम्पियन्स ऑफ क्लीन एयर’ चरण की, शुरुआत 4 दिसंबर 2018 को की गयी है। इसमें देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 वरिष्ठ डॉक्टर और 12 प्रमुख राष्ट्रीय चिकित्सा संघ शामिल हैं। संगोष्ठी में डॉ रोहित भाटिया, डॉ पंकज श्रीवास्तव, डॉ एके वर्मा, डॉ दर्शन बजाज और डॉ अभिषेक कार भी उपस्थित रहे।

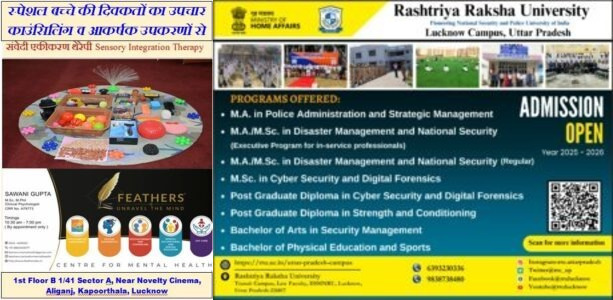
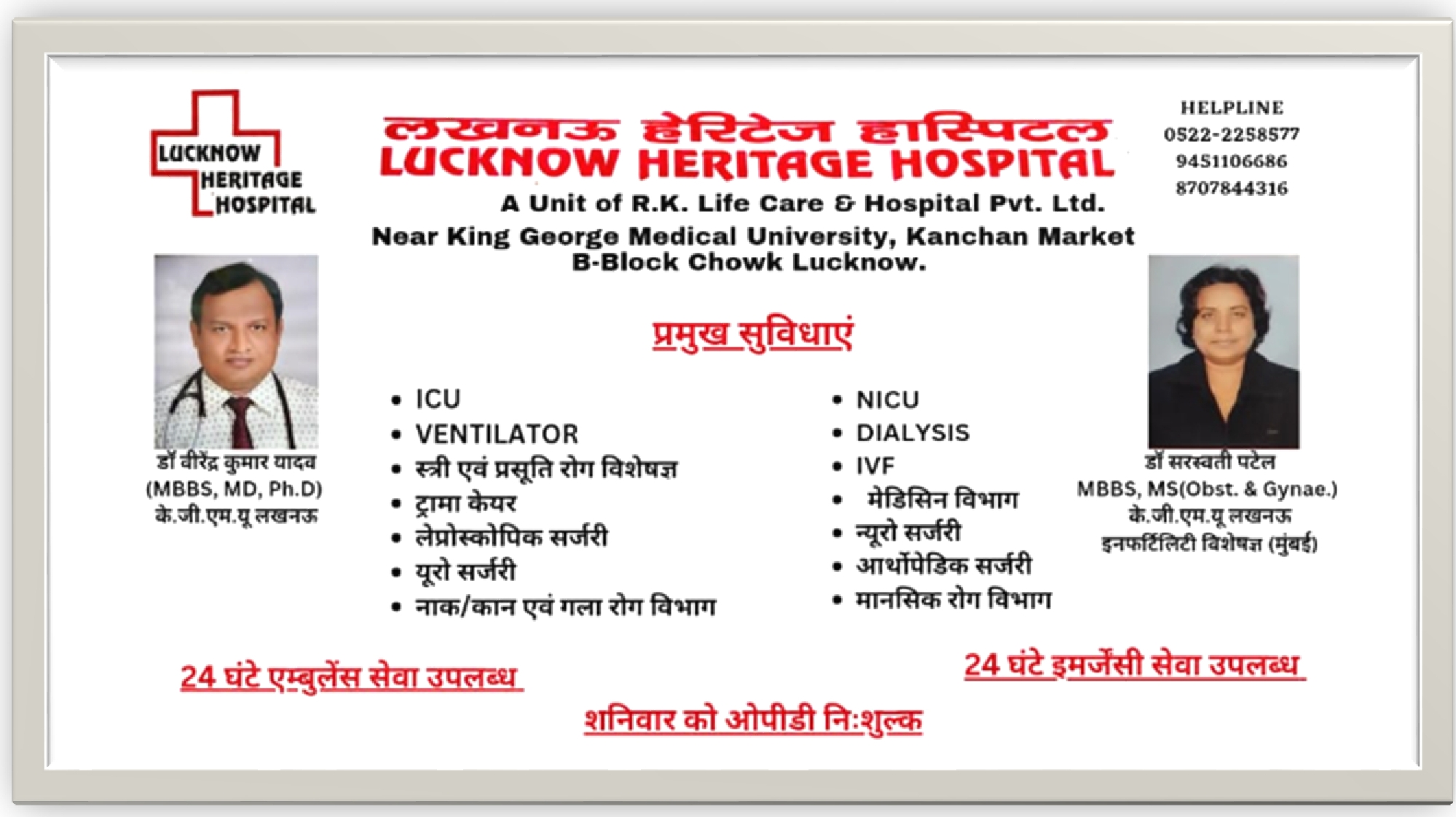
 Sehat Times | सेहत टाइम्स Health news and updates | Sehat Times
Sehat Times | सेहत टाइम्स Health news and updates | Sehat Times






